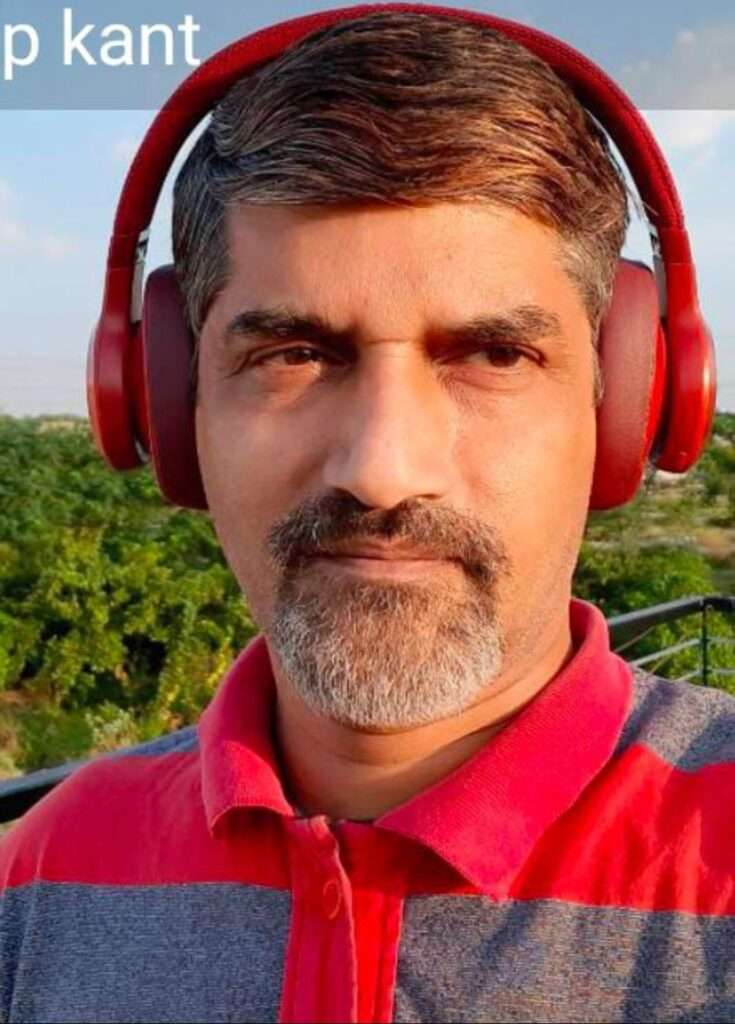पुस्तक समीक्षा : समकाल और सरोकारों की ग़ज़लें
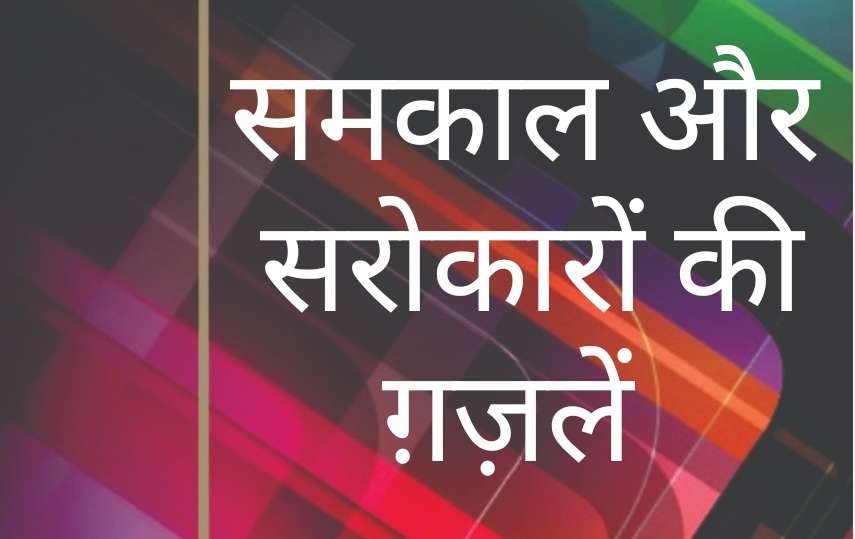

बहते दरिया कहाँ से कहाँ तक गए,
क़ैद अपनी अना में ही तालाब है।
आशीष दशोत्तर के ताज़ा ग़ज़ल संग्रह ‘सम से विषम हुए’ से यह शे’र बयान करता है कि बहाव कितना ज़रूरी है? यह बहाव आपकी स्थिति में बदलाव लाता है – यानि समय के साथ परिवर्तन होना भी आवश्यक है, हाँ यह भी ज़रूरी हो कि यह परिवर्तन सकारात्मक बदलाव लाए । एक और शेर में इसके समानार्थी बात आती है-
तोड़ा है उसी ने तो यहाँ सारी हदों को,
आज़ाद फिज़ाओं में जो बिखरा है हवा सा।

और बिल्कुल! आज़ाद फिज़ाओं में बिखरने वाला ही सब तक पहुँच सकता है, पर ऐसी आज़ादी अगर कोई अपनाए और उस पर पहरा लगा दिया जाए तो! हालांकि ख़ुश्बू पर कौन सा पहरा कामयाब हुआ है, ख़ुश्बू है तो सब तक पहुंचेगी ही। ख़ुश्बू पर न सही लेकिन वे लोग जो शिद्दत के साथ आज़ादी की बात करना चाहते हैं उन पर समाज के तथाकथित ठेकेदारों की पैनी नज़र है। इसलिए परिंदों को निर्देश दिया जाता है कि अपने परों पर खुल कर नाज़ न करें –
सय्याद उन्हें ही तो कभी क़ैद करेगा,
जिन को है बहुत नाज़ यहाँ अपने परों पर।
हे राम, कहाँ दिल में बसाया है किसी ने,
उपयोग मगर राम का भरपूर किया है ।
विधा कोई भी हो, कहानी या कविता, गीत या ग़ज़ल, लेखन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें हमारा समकाल और समाज किस तरह से और कितना दिखता है? इस लिहाज़ से आशीष की ग़ज़लें अपने होने को सार्थक करती नज़र आती हैं । इनमें हमारे इस समय को साफ़ -साफ़ देखा जा सकता है, जिसमे हम किसी चीज़ का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए भरपूर करते हैं।

सबसे बेहतर समाज वही होता है जहाँ रक्षक, रक्षक का ही काम करे, भक्षक का नहीं । और यदि ऐसा है तो उसे समाज से बदतर कोई समाज नहीं । आशीष का ग़ज़लकार हमारे समकाल की इस विद्रूपता को बखूबी पकड़ता है-
महकते फूल बोले गुलसिताँ से,
बचा लेना हमें बस बागबाँ से
डर नाम की यह चीज़ सब जगह हावी है। गाँव में गाँव के गुंडे से भी, तो गाँव के तथाकथित सरदार से भी | वे इसी डर के लिए दरिया और किनारों को प्रतीक बनाकर शेर कहते हैं-
रहना भी इसके साथ है, बहना भी दरमियां
दरिया करेगा कैसे किनारों से दुश्मनी।
समय कोई सा भी हो वर्तमान या भूतकाल या आने वाला भविष्य यह एक अकाट्य सत्य है कि भले लोग ही ठगे जाते हैं, आशीष का ग़ज़लकार इस अकाट्य सत्य को शेर में ढालता है-
दुनिया की नज़र में है जो इन्सान भला सा,
सदियों से कतारों में खड़ा है वो ठगा सा।
आशीष का ग़ज़लकार इस समाज के उस घालमेल की शिनाख़्त करता है जिसके तहत परखा किसी को जाता है और ईनाम किसी और को दिया जाता है-
कहा है आपने सोना किसी को ,
कसौटी पे मगर परखा किसी को।
जीते अगर ये ज़िंदगी उनके हिसाब से,
फिर वो नवाज़ते तुम्हें कितने ख़िताब से।
जो सफे-अव्वल में आने का यहाँ हक़दार था ,
आदमी आख़िर में है वो आज भी बैठा हुआ।
नेकी घटाई आप ने, जोड़ा बुराई को,
सारे समीकरण तभी सम से विषम हुए।
दिखाया जाता है कि यह समय बेहतरीन है और इस से बेहतर स्थितियाँ कभी रही ही नहीं। लेकिन सच क्या यही है जो दिख रहा है? अगर नहीं तो इसे कौन पकड़ेगा और दावे के साथ बोलेगा? साहित्यकार यह काम कर सकता है और करता है| और यही आशीष का ग़ज़लकार हमारे समय की उस चमक को पकड़ता है जिससे हमारी आँखें सिर्फ़ चौंधियाई जा रही है और उस चमक के पीछे के सत्य को नहीं देख पा रही-
ये भी नक्शा तेरे घर का नायाब है,
कच्ची बुनियाद है, ऊंची मेहराब है।
और इसीलिये यह ग़ज़लकार भरोसे पर भी भरोसा न करने को कहता है –
भरोसा न क़ासिद पे इतना करो ,
लिफाफे से चिट्ठी निकल जाएगी।
जैसे समय के बारे में भरम हो सकता है कि इस समय की अच्छाई या बुराई को पहचानना भी मुश्किल हो ठीक वैसा ही आदमी के चरित्र के बारे में भी, कहता कुछ और है पर करता कुछ और, दिखता कुछ और है पर होता कुछ और। यह आशीष के ग़ज़लकार की सफलता है कि वह छद्म किरदारों की पहचान साफ़गोई से कर सकता है-
भलाई के लिए मशहूर हैं वे,
भले किरदार के अच्छे नहीं हैं।
फक़त मेरा नहीं सब का है कहना,
सितम सरकार के अच्छे नहीं हैं।
और यह ग़ज़लकार इसीलिये कहता है कि शऊर की उम्मीद आख़िर हमी से क्यूँ भाई?
कोई तो बदज़ुबान है, कोई है बेहया,
उम्मीद सबको ही रही हमसे शऊर की।
अगर समाज की इतनी सारी विडम्बनाओं, विद्रूपताओं को सामने लाना साहित्यकार का काम है तो जीवन के लिए एक सम्बल देना भी उसी का काम है। साहित्य भी हमें जीने का यह सलीका देता है की बदतर से बदतर परस्थिति में भी जीवन को बिना विचलित हुए बेहतरी से जिया जा सके। इसीलिये उनका ग़ज़लकार आम आदमी को सम्बल देता है-
है कौन यहाँ जिसको कि अवसाद नहीं है,
इक तू ही अकेला कोई अपवाद नहीं है।
हमारे समय का एक भयावह सत्य यह भी है कि हमने कॉन्क्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं और घर के सामने एक पेड़ के लिए भी ज़मीन नहीं बचाई कि सुकून से छाँव में बैठा जा सके। जंगल जो सैंकड़ों साल में अपना रूप ग्रहण करते हैं वे काटे जा रहे हैं और ऐसे गार्डन विकसित किये जा रहे हैं जिनमे सैंकड़ों लीटर पानी भी डाल दिया जाए तो भी छाँव नहीं मिलेगी और बरसात का वातावरण नहीं बनेगा। आशीष का ग़ज़लकार इस विडम्बना को बड़ी खूबसूरती से पकड़ता है-
जंगलों के फ़ोटो से घर हरा भरा क्या हो,
छांव देने वाला तो इक शजर ही काफी है।
रचनाकार सवाल उठाता है। उठाना भी चाहिए, नहीं तो काहे का रचनाकार? आशीष का ग़ज़लकार भी सवाल उठाता है-
ज़रा पूछें कभी उस बदगुमाँ से,
ज़मीं दिखती नहीं क्या आसमाँ से?
इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जाहिल ने क्या किया,
लेकिन मुझे बताइए क़ाबिल ने क्या किया?
बहरहाल, समकाल और सरोकारों से भरपूर आशीष की गज़लें हमें आश्वस्त करतीं हैं कि लिखने की सार्थकता बाकी है।
ग़ज़ल संग्रह : सम से विषम हुए
ग़ज़लकार : आशीष दशोत्तर
प्रकाशक- इंक पब्लिकेशन
मूल्य- 200/-

12/2, कोमल नगर
बरवड़ रोड रतलाम-457001 मो.9827084966